दुःख और तितलियाँ
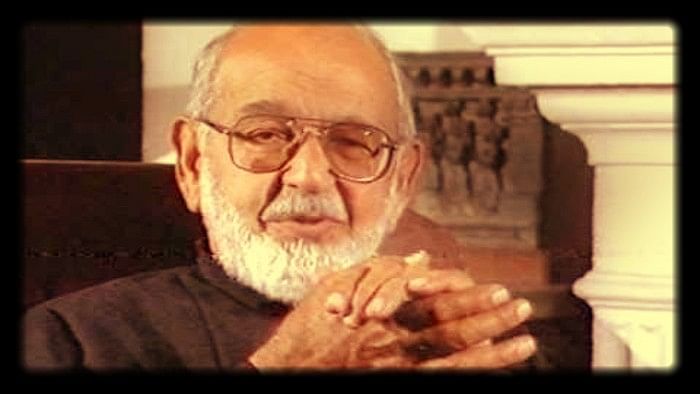
Agyey
1
शेखर उस पहाड़ी से उतरता हुआ चला जा रहा था। उसके क़दम अपनी अभ्यस्त साधारण गति से पड़ रहे थे, वह किसी प्रकार की जल्दी नहीं कर रहा था। क्योंकि यद्यपि वह अपने मन में उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, तथापि उसके भीतर कहीं, उसकी आत्मा के छिपे-से-छिपे स्तर में लिपटी हुई कहीं, इस बात की पूर्ण अनुभूति थी कि वह व्यर्थ जा रहा है क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी है अब डॉक्टर आकर कुछ नहीं कर सकता-सिवाय इसके कि एक क्रिया की जो पूर्ण हो चुकी है, अपने विशेष ज्ञान द्वारा एक और पूर्णता, एक अन्तिमत्व दे दे; – रो पड़ें।
और वह सोच रहा था : हमारे सुन्दर घर की इकाई छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो जाएगी-क्यों? उसका अवश मन भाग-भाग जाता था भूत की ओर – उसके भाई-बहिन के बाल्यकाल की ओर, बहुत पूर्व आबाद किये हुए घरों और स्थानों की ओर, पुराने मकानों की ओर, पुराने फ़र्नीचर की ओर, भूले हुए चित्रों की ओर… और वह इन सब विचारों से लदा हुआ भी, बिना किसी प्रकार की व्यस्तता पा जल्दी के, अपनी अभ्यस्त साधारण गति से चला जा रहा था उस पहाड़ी रास्ते से उतरता हुआ…
एकाएक वह रास्ते के मध्य में रुककर खड़ा हो गया, और एक तीखे फुसफुसाते स्वर में बोला, “वह मर गयी है…” फिर दो-चार क़दम चला और फिर रुक गया।
कौन मर गयी है?
माँ। माँ मर गयी है। माँ मर गयी है…
मर गयी है। क्या अभिप्राय है इसका – मर गयी है?
कोई अभिप्राय नहीं है। कोई अर्थ नहीं है। कुछ नहीं है।
कुछ परवाह नहीं है…
और शेखर फिर उसी गति से चल पड़ा।
पता नहीं, उसने डॉक्टर से क्या कहा। या कैसे कहा। पर कुछ कहा ज़रूर, क्योंकि डॉक्टर ने अमोनिया, ब्राण्डी, इंजेक्शन के लिए एड्रिनलिन और अन्य दवाइयाँ, जो हार्ट-फ़ेल्यर में दी जाती हैं, निकालकर उसे देकर और इंजेक्शन की पिचकारी अपनी जेब में रखते हुए पूछा था, ‘कितनी दूर है?’ और उनका उत्तर, ‘तीन मील है – और चढ़ाई में’, सुनकर कहा था, ‘देर हो जाएगी – यहाँ पहाड़ों में यही तो मुश्किल है।’
वे दोनों उसी रास्ते पर वापस चढ़े जा रहे थे। शेखर की अभ्यस्त गति से भी धीरे, क्यों व्यस्क डॉक्टर धीरे चलता था।
शेखर की डॉक्टर से जितनी बात चलने से पहले हो गयी थी, उतनी ही होकर रह गयी थी, उससे अधिक कुछ नहीं हुई। वे बिलकुल चुपचाप बढ़े जा रहे थे और किसी समय ऐसे जाना अशिष्टता होती; किन्तु इस समय चुप रहने के लिए यही कारण पर्याप्त था कि चढ़ाई में साँस फूल जाती है, बोलना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है।
पर शेखर बोल नहीं रहा था, वह घटना कैसे हुई-पहले-पहल उसे उसका क्या संकेत मिला…
उसे याद आया, वह अपने कमरे में बैठा एक पत्र पढ़ रहा था – अपनी विधवा बहिन का पत्र, जो उसी समय आया था। उसे वह वाक्य भी याद आया, जिसे पढ़ते-पढ़ते उसने अपने पिता की अत्यन्त करुण और विवश करने वाली पुकार सुनी थी – “शेखर, देख तो!” वह वाक्य पता नहीं क्यों, उसकी बहिन ने उसी पत्र में लिखा था; पता नहीं क्यों, वह पत्र उसी समय आया था; पता नहीं क्यों? वह उस समय वही वाक्य पढ़ रहा था जो अब इतना अभिप्राय पूर्ण हो गया है…
‘हमारे वंश में एक परम्परा है कि हममें बहिनें प्रायः निस्सन्तान होती थीं, और इसलिए अपने छोटे भाइयों को गोद ले लेती थीं। और मैं सोचती हूँ कि बहिन जब माँ बनती है, तब माँ से कितनी अधिक हो जाती है…’
क्यों नहीं उसे उसी समय ध्यान आया था कि – कि अब कौन बनेगी उसकी माँ! वह दौड़ा हुआ उस कमरे में गया था जहाँ उसकी माँ कई दिनों से शय्या-ग्रस्त पड़ी थी, और जहाँ उस समय उसके पिता एक विचित्र मुद्रा से अपने सामने पड़े हुए एक क्षीण, मुरझाये हुए और किसी अवाक् पीड़ा से इधर-उधर सिर झटकते हुए अँधेरे को देख रहे थे… शेखर के पहुँचते ही उन्होंने एक प्रश्न-भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। शेखर उसका उत्तर नहीं दे सका। उसने नाड़ी की गति देखी। श्वास की गति देखी। आँखों की पलकें उठाकर देखा। चुप रहा।
पिता ने पूछा, “क्या हुआ?”
विवश कुछ कहना ही पड़ा, “कोलैप्स है!”
“फिर?”
उत्तर में शेखर ने ब्रांडी की बोतल उठायी, थोड़ी-सी एक काँच के गिलास में डाली ओर हाथ से मुँह खोलकर उसमें डाल दी।
वह गले से उतरी नहीं, एक निरर्थक-सी धारा में ओठों से बह गयी।
एकाएक माँ ने फिर आँखें खोलीं। गर्दन फेरकर पति की ओर देखने की चेष्टा करने लगी। गर्दन अधिक नहीं घूमी, तो आँखें फिराकर पति के मुख की ओर देखने लगी! – स्थिर, अपलक और किस उग्र अभिप्राय-भरी दृष्टि से?”
पिता ने टूटती-सी आवाज़ में पूछा – “क्या, कहो क्या होता है?”
शरीर वैसा ही स्थिर, किन्तु एक जड़ता लिए हुए। आँखें उधर ही उन्मुख, अपलक। पर अब चिर-अपलक! उस अभिप्राय से शून्य!
शेखर ने दबे-पाँव बढ़कर पास पड़ी टार्च उठायी, आँखों में उसका प्रकाश छोड़कर पुतली देखी। वह भी शून्य। रिक्त।
ये सब घटनाएँ, सब दृश्य एक-एक करके शेखर के आगे से हो गये-ऐसे, जैसे उसके सामने के पथ पर ही, किसी दीप्त रंगराशि से वे चित्रवत् खींच दिए गये हों…
डॉक्टर ने पूछा, “उनकी आयु कितनी है?”
“कोई पचास।”
“हूँ।”
चुप।
शेखर फिर वहीं पहुँच गया। उसके पिता ने पूछा था, “क्या-” और चुप रह गये थे। और वह किस मुख से उत्तर देता कि क्या…
पिता ने मुँह फेर लिया। शेखर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर माँ की पलकें दाबकर बन्द कर दी; किन्तु वे फिर खुल गयीं-पहले-सी नहीं, अधखुली रह गयीं।
शेखर ने पूछा, “डॉक्टर को बुला लाऊँ?
“अच्छा!”
जिस प्रकार प्रश्न में आशा या निराशा कुछ भी व्यक्त नहीं की गयी थी, उसी प्रकार उत्तर भी पूर्ण संवेदन-शून्य वाणी से दिया गया था। इतनी शून्य कि शेखर सोचने लगा, “क्या ये भी जान गये हैं और मुझसे छिपाना चाहते हैं, या अभी अनभिज्ञ हैं…”
वह उस कमरे से निकला, तो किसी आशंकित भाव से नहीं; उसने कोई इंगित नहीं दिया कि-क्या हो गया है। केवल उस साधारण शीघ्रता से जिससे डॉक्टर को बुलाने जाना चाहिए…
जब शेखर अपने पुकारे जाने से लेकर डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल पड़ने तक सब घटनाओं को देख चुका, तब उसका मन कुछ क्षण के लिए रुक गया। वह बिलकुल शून्य दृष्टि से पथ की ओर देखता हुआ चलता रहा।
उस दिन सवेरे वर्षा दो दिन के बाद थमी थी। शेखर ने देखा, पथ पर अनेकों फिलें, अपनी पीठ पर अपनी ऐहिक सम्पत्ति, अपना घोंघा घर पर लादे हुए अपनी लेसदार मूँछों से पथ टटोलती हुई मन्थर-गति से चली जा रही हैं; जब शेखर गया था, तब भी वे ऐसे ही चली जा रही थी; किन्तु तब कोई उनकी छाप शेखर के मन पर नहीं बैठी थी। अब इन्हें देखकर उसे याद आया, वह तब भी इन्हें देख गया था।
चलते-चलते शेखर ने देखा, एक फिल डॉक्टर के पैर के नीचे आकर कुचल गयी है-डॉक्टर सामने देखता हुआ चल रहा था और शेखर भूमि की ओर। तब शेखर ने यह भी देखा, पथ में अनेक स्थलों पर वैसी अनेक दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, अनेक स्थलों पर एक घिनौनी कीच-सी पड़ी है, जो थोड़ी ही देर पहले एक प्राणी थी-एक प्राणी ही नहीं, एक समूची गृहस्थी, क्योंकि उनका घोंघा-रूपी घर भी तो पीठ पर ही लदा होता है!
शेखर फिर एकाएक रुक गया। उसे ऐसा लगा कि वह कुछ सोचने के लिए रुका है, एक विचार उसके मन में उठने ही वाला है। किन्तु वह उठा नहीं। शेखर ने अपने-आपसे पूछा, “क्या सोचने लगे थे?’ और उत्तर न पाकर, अपने पर नीरस हँसी हँसकर, वह फिर चल पड़ा।
और चलते-चलते उसे विचार आया, हम व्यर्थ ही मृत्यु को इतना तूल देते है…
2
पर घर से कुछ दूर पहुँचकर ही उसे जान पड़ा, वह भूल है। मृत्यु में एक भयंकर यत्परोनास्तित्व है, जो क्षुद्र हो ही नहीं सकता, जो एक व्यक्ति के जीवन से सम्बद्ध होकर भी व्यापक रूप से सर्वत्र छायी है। उसे लगा घर के वातावरण में ही कुछ बदला गया है, एक भीमकाय, दैत्य-सा आकार झूम-झूमकर फुंकार कर रहा है; किन्तु वह फुंकार है शीतल और बिलकुल शब्दहीन, और इसलिए और भी भयंकर!
क्या यह व्यक्ति-संवेदना से उत्पन्न एक भावना-मात्र है? उसके दुख-जनित मोह की परछाई। किन्तु वह तो इस घटना को बिलकुल असम्पृक्त दृष्टि से देख रहा है, उसे तो यह जान ही नहीं पड़ता कि वह किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव कर रहा है! वह तो मानो सम्पूर्णता असंलग्न, निरीह होकर इसकी आलोचना कर रहा है।
उसने दबे-पाँव भीतर प्रवेश किया!
आँगन में कोई नहीं था।
पहले कमरे में भी कोई नहीं था।
कहीं कोई दीख भी नहीं पड़ता था।
शेखर ने चाहा, किसी को पुकारूँ, ताकि सूचना हो जाय कि डॉक्टर साहब आ गये हैं; पर उससे पुकारा नहीं गया।
तीसरे कमरे में शेखर का भाई खड़ा था; पर उसने शेखर से आँख नहीं मिलायी, हिला भी नहीं।
शेखर और डॉक्टर ‘उस’ के साथ वाले कमरे में पहुँचे। वहाँ पिता खड़े थे। देखते ही उन्होंने अँग्रेज़ी में कहा, ‘यू आर टू लेट!” (आप बहुत देर से आये हैं।)
उस नीरस वाणी को सुनकर शेखर के मन में भाव उठा कि उसके पिता अँग्रेज़ी इसलिए बोले हैं कि एक विदेशी भाषा में अपने को छिपा लेना अधिक सहज है। अपनी भाषा का अपनापन हमें अपना हृदय खोल देने को खामखाह विवश कर देता है। और साथ ही उसे विस्मय भी हुआ कि वह कैसे इस समय भी ऐसे बातें सोच सकता है।
पिता के मूक संकेत की अनुमति से डॉक्टर उस कमरे की ओर बढ़ा-शेखर पीछे-पीछे। वहाँ ‘वह’, जो शेखर की माँ थी, एक रज़ाई से पूर्णतया ढँपी हुई पड़ी थी। डॉक्टर ने मुँह पर से रज़ाई हटाई और तुरन्त फिर ज्यों-की-त्यों कर दी।
पिता दूर ही से देख रहे थे। बोले, “हूँ…”
थोड़ी देर एक बोझिल-सा मौन रहा। फिर डॉक्टर ने कहा, “कारण हार्टफेल्यर ही रहा होगा।” तपेदिक था तो-
पिता ने कहा “नहीं, तपेदिक नहीं था-”
डॉक्टर ने शेखर की ओर इशारा करते हुए कहा, “मुझसे यह कह रहे थे”
“नहीं, पहले वह ख़याल था, किन्तु बाद का डायग्नोसिस (निदान) उसके विरुद्ध था।”
फिर एकाएक बिखरते हुए-से स्वर में, “पर इससे अब क्या – मृत्यु मृत्यु है…”
थोड़ी देर फिर स्तब्धता। शेखर ने चुपचाप दवाइयाँ इत्यादि डॉक्टर को दे दीं। डॉक्टर ने शेखर के पिता की ओर देखते हुए, कुछ झिझकते हुए कहा, “मैं अत्यन्त दुखी हूँ।” आप-” और चुप गया। क्षण-भर बाद वह चला गया। फ़ीस उसने नहीं ली।
शेखर उसे दरवाज़े तक छोड़कर लौटा, तो फिर कमरे में पिता बैठे थे, उसके दरवाज़े पर आकर खड़ा रहा। बहुत देर खड़ा रहा। तब एकाएक पिता उसकी ओर देखकर बोले, “खड़े क्यों हो जाओ, कुछ करो।” फिर कुछ कठोर, कुछ चिड़-चिड़े स्वर में, “अब क्या फ़ायदा है। अब लौटकर थोड़े ही आएगी। वह तो गयी अब। वह तो मर गयी। अब क्या। वह तो मर गयी…” और दृढ़, ललकार भरी-सी चाँप से, मानो पृथ्वी को दबाते हुए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे।
और पिता के वाक्यों में ‘मर’ शब्द पर दिया हुआ ज़ोर बार-बार उसके मन में गूँजने लगा। मानो उसके हतसंज्ञ मस्तिष्क पर मृत्यु की अगाध, अच्छेद्य अतिमाता की छाप बिठा देने का व्यर्थ प्रयत्न करता हुआ।
3
घाटी पर उतरकर, उसकी तलहटी के छोर पर ही, एक छोटा-सा पत्थरों से चुना हुआ चबूतरा। ऊपर छिड़का हुआ पानी। उससे ऊपर लकड़ी से चुना हुआ एक और चौकोर स्तूप, जिसमें लकड़ी के भीतर से लाल और श्वेत वस्त्रों की झाँकी मिल जाती है। पास में पड़ा हुआ मटका-भर पानी, और एक बड़े-से थाल में हवन-सामग्री।
कुछ दूर पर शेखर के पिता, भाई और कई-एक लोग। दूसरी ओर शेखर अकेला।
उसके बाद एक तन्द्रा। एक गतिमान तन्द्रा, जिसमें कोई भी निश्चल नहीं बैठता, सभी कुछ-न-कुछ करते जाते हैं; पर कोई जानता नहीं कि क्या हो रहा है।
केवल जब चिता जलने लगी, तब मन्त्रोच्चार के साथ-साथ एक लम्बे हत्थेवाले स्रुवा से उसमें घी की आहुति डालते हुए शेखर को याद आया, जब चिता चुनी जा रही थी, सारा शरीर ढका जा चुका था, केवल मुख ढकना बाकी रह गया था, तब उसके पिता ने आकर एकाएक कहा था, “एक फ़ोटो ले लेते-” पर सब ओर से मौन पाकर, स्वयं भी कुछ देर मौन रहकर प्रश्न-सूचक आवाज़ में कह दिया था, “क्या करना है…” तब शेखर ने दबे स्वर में कहा था, “क्या करना है…” यद्यपि स्वयं उसके मन में भी यह बात उठी थी कि फ़ोटो ले लेना चाहिए। तब पिता ने धीरे से एक लज्जित-सी हँसी हँसकर-मानो अपनी कोई कमजोरी प्रकट करते हुए लज्जित हों पर रह भी न सकते हों-कहा था, “मुख तो देखूँगा ज़रूर…”
पता नहीं, वह कैसे क्यों हुआ कि बहुत कोशिश करने पर भी कपड़ा नहीं हट सका। ऊपर जो सूत लपेटा गया था, वह खोला गया; पर कपड़ा कहीं लकड़ी में अटक गया था, नहीं छूटा, नहीं छूटा। पिता ने फिर एक हँसी – किस-किस कुछ को ‘हँसी’ कहा जा सकता है! – हँसकर उसे छोड़ दिया और पीछे हट गये।
शेखर सोचने लगा कि उस समय उनके मन पर क्या बीती होगी। पर क्यों? उसके अपने मन पर उस घटना का क्या प्रभाव हुआ था? कुछ नहीं, उस समय तो प्रभाव के लिए अवकाश कहाँ था; प्रभाव तो बाद में होगा, जब उस सब-कुछ की तात्कालिक उग्रता कम हो जाएगी, जब वह जड़ बनानेवाली न रहकर केवल रुलानेवाली रह जाएगी…
शेखर को पता नहीं था कि उसके हाथ उस लम्बे स्रुवा को उठाये-उठाये थक गये हैं, पर तभी उसके पीछे भाई ने वह उसके हाथ से ले लिया। शेखर घाट के उतार पर ही बैठ गया, और अपलक-नयन चिता की ओर देखने लगा।
उन लपलपाती जिह्वाओं में, उन असंख्य रक्त-मुकुरों में, उसे माँ की साधारण सौम्य मूर्ति का प्रतिबिम्ब नहीं दीखा। दीखे भूत के चित्र, वार्तालाप, भाव, जो थोड़ी देर में एक भयंकर स्मृति में परिणत हो गये – एक स्मृति जो साकार उसके आगे नाचने लगी और हटाये नहीं हटी…
वह दृष्टि-माँ उस अन्तिम क्षण में पिता की ओर देख रही… क्यों? क्या कहने को? उस अन्तिम एक क्षण में, ऐसी कौन-सी बात उसे याद आ गयी थी जो वह अपने तीस वर्ष के वैवाहिक जीवन में नहीं कह चुकी थी, जिसका इसी समय कह डालना इतना महत्त्वपूर्ण हो गया था – मृत्यु के अन्तिम, अमोघ आघात से भी अधिक महत्त्वपूर्ण? क्या यही मात्र कहना चाहती थी कि वह आघात अन्तिम है, अमोघ है, कि अब…
अब क्या?
शेखर भूल गया कि वह किस भाँति वाक्य को पूरा करना चाहता था। वह उसी दृश्य में खो गया, उसी समय की विकार-मालाएँ फिर उसके मन में भर गयीं। उसे याद आया, उसी समय उस दृष्टि को देखकर उसके मन में एक तूफ़ान-सा उठा था-विचार आये थे लहरों की तरह, एक के ऊपर एक, किसी एक ही गति से प्रेरित किन्तु परस्पर-असम्बद्ध। उसने मन-ही-मन में, किन्तु खिंचे हुए स्वर में कहा था-
‘माँ, माँ, तुम्हारी दृष्टि क्या मेरे लिए नहीं है? किसी और के लिए नहीं? किसी वस्तु के लिए नहीं? केवल, मात्र उसी के लिए वह अचल, शब्दहीन सन्देश…?
ओफ़, वह इस सन्देश को भस्म कर देनेवाली तीक्ष्णता के आगे झुक क्यों नहीं जाता, नष्ट-भ्रष्ट, क्षार क्यों नहीं हो जाता! कहता जाता है, ‘पथरायी जा रही हैं – पथराती हैं -यह क्या हो रहा है…’
वह क्रोध था या और कुछ, जिससे अभिभूत होकर शेखर ने ज़ोर से अपना मुँह बन्द कर लिया था ताकि ओठों पर आये हुए शब्द न निकल जाएँ?-
“मूढ़ सुना, वे क्या कहती हैं, सुनो; यह शिकायत फिर भी हो सकेगी-बाद में; अभी उनका सन्देश मत खोओ…”
तब फिर, रिक्त! तब वह खिंचाव नष्ट हो गया था, और वह डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करते हुए एक शान्त भाव से सोचने लगा, माँ को सम्बोधित करके कहने लगा था, “माँ, अब निर्जीव शरीर-मात्र, उस एक दृष्टि से तुमने सब-कुछ कह दिया है, तुमने अपना जीवन समाप्त किया है एक अन्तिम दिव्य सौन्दर्य-मयी मुद्रा में! तुम माँ रही हो, तुम्हारा जीवन अपनी सन्तान में और गृहस्थी की सैकड़ों-हजारों छोटी-छोटी उलझनों में फँसा रहा है; किन्तु तुम्हारी प्रकृति के घोरतम तल में कुछ था, जो माँ नहीं, स्त्री था; जो उसका था, उसका रहा और अब सदा के लिए रहेगा… मृत्यु क्या है? पारलौकिक जीवन क्या है? स्मृतियाँ, श्रुतियाँ क्या हैं? ईश्वर क्या है? मान लिया कि तुम मर गयीं, सम्पूर्णतया नष्ट, बिलकुल लुप्त, निःशेष हो गयीं। उससे क्या होता है? तुमने वह कह दिया है…”
शेखर एकाएक उठा खड़ा हुआ। एक बार उसने अपने चारों ओर देखो, मन्त्रोच्चार करते हुए भी तीन-चार जन उसी की ओर देख रहे थे उसने अपने भाई स्रुवालेलिया और यन्त्रवत चिता में थी डालने लगा। अब चिता जल भी चुकी थी, राह-संस्कार समाप्त हो चुका था, तब भी कुछ देर शेखर को होश नहीं हुआ। उसके बाद ह एकाएक चौंका-सा और चारों ओर देखकर, लज्जित-सा होकर, स्रुवा रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसके पिता ने कहा,”अब क्या है शेखर, अब चलो।” तो बिना लौटकर देखे भी चल पड़ा। पीछे-पीछे पंडित लोग और अन्य लोग आये, सबसे पीछे पिता, दो-एक बार लौट-लौट कर देखकर, चोरी से आँखें पोंछकर!
किन्तु शेखर की आँखें? निर्निमेष। गम्भीर, हर चिन्ताहीन। किसी भी प्रकार की अनुभूति से हीन। वह उस सारे जुलूस (!) के आगे-आगे चला जा रहा था..
4
पथ पर।
मन्दिर के पथ पर, जहाँ पहुँचकर यह समूह बिखरेगा; जहाँ जाकर अनन्तपथ-पथिक की अन्तिम झाँकी लेकर, फिर उसे भुलाया जाएगा, सदा के लिए जीवन की परिधि के बाहर धकेलकर उससे अलग कर दिया जाएगा।
उस समय तक वह माँ है, स्त्री है, मानवी है, अपनी है; उस समय वह हो जाएगा – एक स्मृति।
शेखर सोच रहा है कि लोग मन्दिर क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं? वह स्वयं जाता रहा है; किन्तु वह जाता रहा है वहाँ का संगीत सुनने, वहीं के समवेत आरती-गान की श्रद्धा-भरी ध्वनि के कम्पन से एक अकथ्य अनुभूति प्राप्त करने, जो मन्दिर के बाहर, देवस्थान के बाहर, कहीं नहीं प्राप्त होती-या किसी असाधारण अवसर पर ही प्राप्त होती है। वह जाता है उस अनुभूति को प्राप्त करने ही नहीं, उस कोमल झुटपुटे में चुपचाप उसे दृढ़ करने, धूप-धूम्र, सुमन-सौरभ और घंटानाद से सजीव उस रहस्यपूर्ण वातावरण में उसका संचय करके उसे साथ ले आने के लिए। क्या अन्य लोग भी इसी भावना से जाते हैं?
वह देखता है कि इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता-न उसके साथ जाने वालों के चेहरों में, न उनकी वाणी में, न उनकी बातचीत में।
उस भीड़ में कई ऐसे भी हैं जो अपने को शेखर का सम्बन्धी बताते हैं। यही उनका शेखर से सम्बन्ध है। अन्यथा शेखर के पुरखों के वे चाहे कुछ रहे हों, शेखर उन्हें न जानता है, न मानता है, न उनसे किसी प्रकार की निकटता का अनुभव ही कर सकता है। वह उनकी बातें सुनता जाता है और अधिकाधिक विस्मय में सोचता जाता है कि यदि ये मनुष्य हैं, तो क्या मैं ही कोई पशु हूँ, या प्रेत हूँ, जो इनकी दृष्टि से देख नहीं सकता!
“कैसी दर्दनाक मृत्यु है! मरते वक्त एक शब्द भी नहीं कह सकी। हमारा सारा कुनबा बिखर गया। माली बाग़ लगाकर छोड़ गया। उसकी रेख-देख कौन करेगा? बेचारी ने कुछ सुख भी नहीं देखा, मरते वक्त कोई बात भी तो नहीं कह सकीं। अब घर कौन सँभालेगा? किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ क्या है। जानेवाली तो गयी। कुछ कह ही जाती। मृत्यु तो हर एक को ही आती है, पर ऐसी मृत्यु! बिना एक शब्द कहे मर जाना! हरे राम!”
शेखर चुपचाप सुनता है। पर ज्वालामुखी के उबलते हुए लावा के उफान की भाँति उसके भीतर कुछ उठता है, उठता रहता है। यदि वह कुछ कह भी पातीं, तो क्या कह पातीं? कुछ-एक निरर्थक शब्दों के अतिरिक्त क्या? मृत्यु की इतनी बड़ी महत्ता के आगे – क्षुद्र! उनसे होता क्या – अब जब वह मर ही चुकी? वह मर ही चुकीं, तो उनके कहे हुए, या उनके द्वारा कहे जा सकनेवाले, किसी भी शब्द से क्या – किसी भी शब्द से! अब इस सबसे क्या…
फिर कहीं कोई कह रहा है-
“सुना है, मरते समय उनकी कुछ खातिर भी नहीं हो सकी। उसी दिन सवेरे उन्होंने एक पान माँगा था – वह नहीं मिल सका। वे यह कहती ही मर गयीं कि मेरे लिए एक पान का भी प्रबन्ध नहीं हो सकता-देखो न उनकी दशा-”
शेखर को एकाएक वह क्षण याद आया, जब उसके पिता ने उससे पूछा था, ‘क्या-?’ और उसने कहा था, ‘कोलैप्स है…’ और उसके थोड़ी देर बाद पिता ने फिर पूछा था-इस बार अंग्रेजी में-‘इज़ देयर लाइफ़? (जीवन, शेष है?)’ और वह चुप रह गया था-यह सोचकर कि शायद शेष नहीं है, और कैसी परिस्थिति में खोया है – एक अन्तिम क्षुद्र शिकायत लेकर कि मेरे लिए पास नहीं आ सका… ईश्वर!
शेखर ने एक लम्बी साँस ली। पर उसे दुख नहीं मालूम हुआ। उसने बात कहनेवाले व्यक्तियों की ओर देखा। एकाएक क्रोध से उसका बदन जल उठा; पर वह ओठ काटकर उसे दबा गया। ओठ से ख़ून निकल आया…
शेखर की गति धीमी हो गयी। अभी तक सारी भीड़ उसके पीछे थी, अब धीरे-धीरे आगे निकलने लगी। एक-आध व्यक्ति ने चाहा, उसे ढाढस दिलाये और आगे चलने के लिए कहे, पर उसके मुख की ओर देखकर किसी को साहस नहीं हुआ।
शेखर की गति क्रमशः और भी धीमी होती गयी…
5
शेखर अभी मन्दिर से बहुत इधर ही था जब सारी भीड़ उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गयी, और वह चुपचाप लौटकर चला आया उसीके अवशेष के पास।
क्रोध कहीं उठता है, और किधर-किधर बहकर कहाँ पहुँच जाता है! इस समय शेखर अपने ही को कह रहा था – “यदि तुम्हारा दुःख उनसे भिन्न है, यदि तुम्हारी अनुभूति उनसे तीखी, उनसे गहरी है, तो तुम ऐसे निर्वेद क्यों हो? तुम्हें क्यों क्लेश नहीं होता, तुम क्यों नहीं रोते? या तुम्हारा दुःख रोने से परे है, तो क्यों नहीं तुम वज्राहत की तरह पड़े हो? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, रत्ती-भर दुःख नहीं हुआ, तुम यहाँ चिता के किनारे खड़े भी सुस्थचित्त यह सोच सकते हो कि तुम्हें दुःख हुआ या नहीं? दिव्य पुरुष तुम नहीं हो; तब पशु, या पत्थर…”
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका मस्तिष्क ठीक काम कर रहा था, किन्तु वह सारा काम था निष्फल, किसी परिणाम तक पहुँचने में पूर्णतया असमर्थ; बिलकुल व्यर्थ।
शेखर चिता की ओर देखने लगा। वह अभी तक सुलग रही थी और जहाँ शेखर बैठा था, वहाँ तक उसका ताप पहुँचता था।
उसमें से धुआँ निकल रहा था; पर एक उत्तप्त वाष्प-सा उठ रहा था, जिसके कारण उसके पार का दृश्य शेखर की दृष्टि में एक विशेष प्रकार से कम्पित हो रहा था, मानो अधूरा जीवन पाकर लड़खड़ा-सा रहा हो…शेखर उसी को देख रहा था, मुग्ध-सा, मूढ़-सा, ऐन्द्रिय अनुभूति से परे कहीं।
एकाएक किसी ओर से तितलियों का एक जोड़ा उड़ता हुआ आया, सीधा चिता की ओर। शेखर ने देखा, वे चिता के पास आकर, शायद गर्मी का अनुभव करके, एकाएक ऊपर उठीं, किन्तु उठते-उठते उस उत्तप्त वाष्प के घेरे में आ गयीं; निकलने की चेष्टा में उद्भ्रान्त इधर-उधर लड़खड़ायीं, फिर काँपकर, मुरझाकर झड़ती हुई पंखुड़ी की भाँति, चिता में गिर गयीं। जल गयीं।
शेखर ने किसी अपर इन्द्रिय से यह सब देखा। उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। एक छोटे-से क्षण में उसके मन में एक भाव गुजरा कि यह घटना भी उस-जैसी है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। पर यह कितनी निरर्थक है, उसके अनुभव निरर्थकता के कारण! इनके मर जाने पर, इनका क्या रह गया होगा? घर-बार? यश? कीर्ति? कृतियाँ? स्मृतियाँ? संतान रही होगी, किन्तु उस मस्तिष्कहीन, ज्ञानशून्य सन्तान को इससे क्या कि वह किससे पैदा हुई थी! कितनी साधारण, कितनी निरर्थक, कितनी क्षुद्र, प्रकृति गति में कितनी नगण्य घटना है यह मृत्यु!
शेखर को अनुभव कुछ भी नहीं हुआ। पर वह लड़खड़ाकर बैठ गया, एक बड़ा सा बुलबुला-सा उसकी छाती में उठा और गले में आकर फूट गया, आँखें उमड़ आयीं; और एक व्यथा-भरी सिसकी में वह रो पड़ा – “माँ!”
(डलहौज़ी, अगस्त 1934)



![kuber chalisa[1]](https://mobihangama.com/wp-content/uploads/2022/09/Kuber-Chalisa1-300x225.jpg)