खितीन बाबू
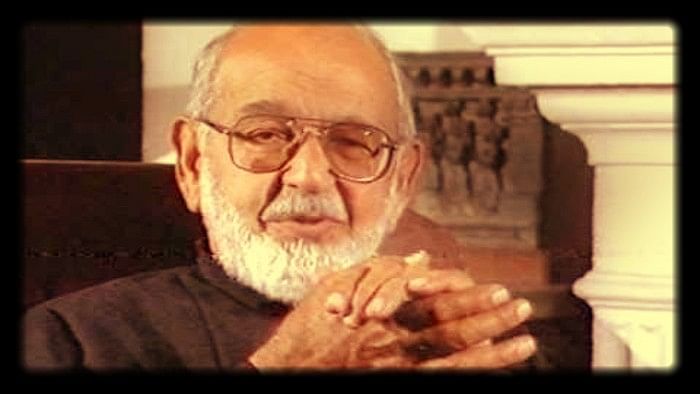
Agyey
वो चेहरे। कौन-से चेहरे? कौन-सा चेहरा? जो जीवन-भर चेहरों की स्मृतियाँ संग्रह करता आया है, उसके लिए यह बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकालकर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता : क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल ही नहीं सकता-फिर वह चेहरा मनुष्य का न होकर चाहे पशु-पक्षी का ही क्यों न हो… यूरोपीय का हर हिन्दुस्तानी चेहरा एक जान पड़ता है; हिन्दुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक। मानव को सब पशु एक-से दीखते हैं। वह भी एक तरह का देखना ही है। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है, वह जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और हर चेहरा स्मरणीय। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आँखें रखते हों।
मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ, तो और अनेक चेहरे सामने आकर उलाहना देते हैं, ‘‘क्या हम नहीं? क्या हमें तुम भूल गये हो?’’ उनमें पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं; इतर प्राणियों में घोड़े हैं; कुत्ते हैं, तोते हैं, एक गिलहरी है, जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी; एक मुनाल है, जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मीलों दौड़ा था; एक कुत्ता है जो मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आँसू गिराता था; एक टूटी चोंच और कटे पँख-वाला कौआ, है जो मुल्तान-जेल में मेरा दोस्त बना था और ‘परकटे’ नाम से पुकारने पर आधा उड़ता और चमकता हुआ आकर हाजिर हो जाता था-कहाँ तक गिनाया जाए, पेड़-पौधों के हम चेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े होते। कालिदास ने शकुन्तला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियों का वर्णन किया है :
‘‘अपसृताण्डुपत्रा मुञ्चति अश्रु इव लताः।’’
मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है -सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय। अगर एक चुनता हूँ, तो किसी असाधारणत्व के लिए नहीं। चुनता हूँ एक अत्यन्त साधारण व्यक्ति का अत्यन्त साधारण चेहरा; क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ – असाधारण ही स्मरणीय नहीं है, हर गुदड़ी में लाल है, ज़रा उसे लौट कर झाँकने का कष्ट तो करो।
वो चेहरे। वह एक चेहरा। खितीन बाबू का चेहरा न सुन्दर था, न असाधारण; न वह ‘बड़े आदमी’ ही थे – साधारण पढ़े-लिखे साधारण क्लर्क। मैंने पहले-पहल उन्हें देखा, तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी। इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने के लायक़ था; चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आँख गायब थी और एक बाँह भी नहीं थी-कोट की आस्तीन पिर लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गयी थी। काने का अपशकुन तो मानते हैं, अति चतुर भी मानते हैं; पर खितीन बाबू की हँसी में एक विलक्षण खुलापन और ऋजुता थी, इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा, तो मालूम हुआ, आँख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी, बाँह पेड़ से गिरने पर टूट गयी थी और कटवा देनी पड़ी। उनके हँसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे।
मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर हो गयी थी। मैं दोरे पर जानेवाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। दो-तीन महीने घूम-घामकर फिर आया; लेकिन खितीन बाबू के दर्शन कोई छह महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ हुए – अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहे थे, वहाँ से बैसाखियों का उपयोग सीखकर बाहर निकले थे।
उनके लिए घटना पुरानी हो गयी थी, मेरे लिए तो एक नयी सूचना थी। मैं सहानुभूति प्रकट करना चाहता था; पर झिझक भी रहा था, क्योंकि किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है; कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा, ‘‘आइए, आइए, आपको अपने नये आविष्कार की बात बतानी है।’’ उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगुनी हो जाती है। वैसी ज़ोर की पकड़ जीवन में एक-आध बार ही किसी हाथ से पायी होगी। मैं बैठ ही रहा था कि वे बोले, ‘‘देखा आपने, कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है? मैंने टांसिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई; एपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया; केवल उसका दर्द गया। भगवान औघड़ दानीं हैं न, सब-कुछ फालतू देते हैं – दो हाथ, दो कान, दो आँखें! अब जीभ तो एक है; आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है?’’
मैं अवाक् उन्हें देखता रहा। पर उनकी हँसी, सच्ची हँसी थी, और उनकी आँखों में जीवन का जो आनन्द चमक रहा था, उसमें कहीं अधूरेपन की पंगुता की झाई नहीं थी। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे बताई थी; यह ठीक याद नहीं कि वह इसी दूसरी भेंट में या और किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है, और उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई होगी उन्होंने थोड़ी-थोड़ी करके दो-तीन किस्तों में।
तीसरी बार मैंने देखा, तो वे दूसरी बाँह भी खो चुके थे। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय गिर गये थे; कोहनी टूट गयी थी और फिर घाव दूषित हो गया, जिससे कोहनी से कुछ ऊपर से बाँह काट दी गयी। इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई-घर में। मित्र-पत्नी भोजन बना रही थीं, और खितीन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन व्यंजन कैसे बनेगा। वे खाने के शौकीन तो थे ही, खिलाने का शौक उन्हें और भी अधिक था, और पाकविद्या के आचार्य थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, लेकिन था यही कि खितीनदा बच गये और अस्पताल से लौट आए; क्योंकि इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटापन्न रही थी। खितीनदा भी इस बात को समझ गये थे, तभी उन्होंने कहा था, ‘‘दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रहा; पर दूँगा मैं और सब-कुछ मैं ही बनाऊँगा।’’ और खुलासा यह किया था कि वे रसोईघर में बैठकर सब कुछ अपनी देख-रेख में बनवाएँगे, बनाएँगी, गृहपत्नी मगर विधान खितीन बाबू का होगा। मित्र ने यह बात सहर्ष मान ली थीं। खितीन बाबू का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था।
मैं एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गया। निमन्त्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था। मैंने गृहपत्नी से पूछा, ‘‘क्या बना रही हैं?’’ और उन्होंने उत्तर दिया, ‘‘मैं क्या बना रही हूँ, बना तो खितीनदा रहे हैं।’’ इस पर खितीनदा बोले, ‘‘हाँ; मेरा छुआ हुआ आप खा तो लेंगे न!’’ और ठहाका मार कर हँस दिए। उनका छुआ हुआ आप तो लेंगे न!’’ और ठहाका मार कर हँस दिए। उनका छुआ हुआ, जिनके दोनों हाथ नदारद! फिर बोले, ‘‘आपने भोजन-विलासी और शय्या-विलासी की कहानी सुनी है?’’
मैंने नहीं सुनी थी। वे सुनाने लगे। एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में आए। पूछने पर एक ने कहा, ‘मैं भोजन-विलासी हूँ।’’ यानी? यानी राजा जो भोजन करेंगे, उसे पहले चखकर वह बताएगा कि भोजन राजा के योग्य है या नहीं। जाँच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया; थाली पास आते-न आते भोजन-विलासी ने नाक बन्द करते हुए चिल्लाकर कहा, ‘‘उं-हूँ-हूँ,ले जाओ; इसमें मुर्दे की बू आती है!’’ बहुत खोज करने पर मालूम हुआ, जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आये थे, उसके किनारे के पेड़ से में एक मरा हुआ पक्षी टँगा था! भोजन-विलासी को नौकरी मिल गयी। शय्या-विलासी ने बताया कि वह राजा के बिछौने की परीक्षा करेगा। उसे शयन-कक्ष में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर जरा बैठा था कि कमर पकड़कर चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ, ‘‘अरे रे, मेरी तो पीठ में बल पड़ गया, क्या बिछाया है किसी ने!’’ सबसे देखा, कहीं कोई सलवट तक न थी, सब गद्दे-वद्दे उठाकर झाड़े गये, कहीं कुछ न था जो विलासी की कमर में चुभ सकता-पर हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था! इस प्रकार शय्या-विलासी को भी नौकरी मिल गयी।
कहानी सुनाकर खितीन बाबू बोले, ‘‘वह भी क्या जमाने थे!’’
मित्र-पत्नी ने कहा, ‘‘आप उन दिनों होते, तो क्या बात होती?’’
खितीनदा ने कहा, ‘‘और नहीं तो क्या। मैं होता, तो राजा को दो नौकर थोड़े ही रखने पड़ते?’’
मित्र-पत्नी ने मेरी ओर उन्मुख होकर कहा, ‘‘खितीन बाबू गाते भी बहुत सुन्दर हैं।’’
खितीनदा फिर हँसे। बोले, ‘‘हाँ-हाँ संगीत-विलासों की नौकरी भी मैं ही कर लेता न?’’
चार बजे भोजन तैयार हुआ; हम आठ-दस आदमियों ने खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी बनी है।
तब लगातार दो-चार दिन उनसे भेंट होती रही; पर उसके बाद मैंने खितीन बाबू को एक बार और देखा, एक लम्बी अवधि के बाद। और अब की बार उनकी दूमरी टाँग भी मूल से गायब थी।
दोनों हाथ नहीं, दोनों टाँगें नहीं, एक आँख नहीं। टांसिनल, एपेंडिक्स वगैरह तो, जैसा वे स्वयं कहते, रूंगे में चढ़ा दी जा सकती हैं। केवल एक स्थाणुः बैठक में गद्देदार मूढ़े पर बैठा था। घर तक वे एक विशेष पहियेदार कुर्सी में लाये गये थे, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी; क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था, और यहाँ वे बिलकुल सहज भाव से बैठे थे। मानो किसी स्वप्नाविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर से मस्तक और कँधे तो पूरे गढ़ दिए हों, बाकी स्तम्भ अछूता छोड़ दिया हो।
मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया – वे कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के सम्बन्ध में की गयी अपनी बहसें याद आ गयी। आत्मा है, तो शरीर में व्याप्त है, या किसी एक अंग में रहती है? अगर सारे शरीर में, तो, कोई अंग कट जाने पर क्या होता है? अपनी थ्योरी याद आ गयी, जिसमें इस पहेली को हल कर दिया गया था, कि जब कोई अंग कटता है, तो उसमें से आत्मा सिमट कर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। यह थ्योरी कहाँ तक मान्य है, इस बहस में तो वैज्ञानिक पड़ें, पर उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलन्त होकर सामने आ जाती थी, उनकी आत्मा न केवल पंगु नहीं थी, वरन् शरीर के अवयव जितने कम होते जाते थे, उसमें आत्मा की कान्ति मानो बढ़ती जाती थी मानो व्यर्थ से सिमट-सिमटरकर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पुंजित होती जाती-सारे शरीर में भी नहीं, एक अकेली आँख में – प्रेतात्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में निष्कम्प दिपते हुए एक आकाश-दीप के समान…
तभी खितीन बाबू ने मुझे देखा। छूटते ही बोले, ‘बोले छिलाम, बेचे, थाक्ते वेशि किछु लागे न!’’ (मैंने कहा था, बच रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए!) और हँस दिए।
इसके बाद मैंने फिर खितीन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुन रहा, सच्ची बात सुना रहा हूँ। तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन सुनने वाले की कमी में कहानी नहीं रुकती, देखने वाला न होने से जीवन-नाटक बन्द नहीं हो जाता। मैंने भी सुनकर ही जाना, खितीन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुँचकर ही पूरी हुई, टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर-ठेले से टकरा गयी थी, वे नीचे आ गये और गाड़ी का पहिया उनके कन्धे के ऊपर से चला गया-बाँह का जो ठूँठ बचा हुआ था, उसे भी चूर करता हुआ। वे अस्पताल ले गये, बाँह अलग की गयी और कन्धे की पट्टी हुई, ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्होंने पूछा कि कन्धा है या नहीं? फिर कहा ‘‘जाना गेलो, ऐटा छाड़ाओ चले!’’ (मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है!) लेकिन अबकी बार वह चलना अधिक देर तक नहीं हुआ; अस्पताल में वे नहीं निकले। शरीर में विष फैल गया था और भोरे में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गयी।
खितीन बाबू : एक साधारण क्लर्क : साधारण दुर्घटना : मृत्यु हो गयी। लेकिन क्या सचमुच? अब भी उन्हें देख सकता हूँ। कभी लगता है कि जिसे देखता हूँ वह केवल अंगहीन ही नहीं है। मानो अशरीरी है, केवल एक दीप्त-अंगों से क्या? अवयवों से क्या? ‘‘जाना गेलो, ऐटा छाड़ाओ चले’’-इस सबके बिना काम चल सकता है। केवल दीप्ति : केवल संकल्प-शक्ति। रोटी, कपड़ा, आसरा, हम चिल्लाते हैं, ये सब ज़रूरी हैं, निस्सन्देह जीवन के एक स्तर पर ये सब निहायत ज़रूरी हैं, लेकिन मानव-जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा यह नहीं है; वह है केवल मानव का अदम्य, अटूट संकल्प…
(दिल्ली, अगस्त 1957)



![kuber chalisa[1]](https://mobihangama.com/wp-content/uploads/2022/09/Kuber-Chalisa1-300x225.jpg)