साँप
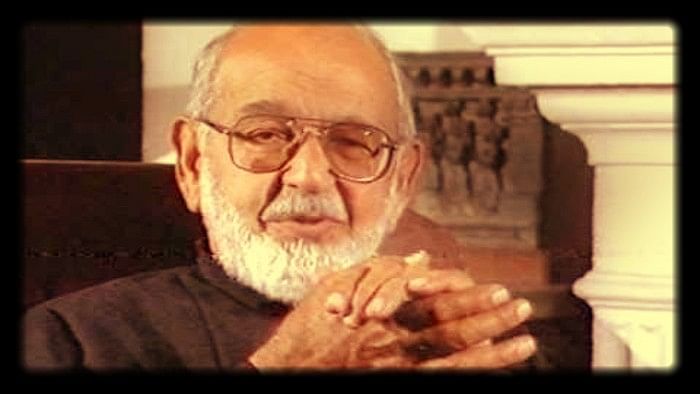
Agyey
अच्छाई-बुराई की बात मैं नहीं जानता। कम-से-कम इतनी नहीं जानता कि सबके, और खासकर अपने, बारे में यह फैसला कर सकूँ कि हम अच्छे हैं कि बुरे। लेकिन उसके बिना जी न सकें, चल न सकें, चाह न सकें, ऐसा तो नहीं है! उसके लिए जानता हूँ कि वह अच्छी है। और यह भी जानता हूँ कि इस बात को जाने रहना, पकड़े रहना जरूरी है कि वह अच्छी है।
सवेरे-सवेरे उससे मिलने गया था। यों तो अक्सर हम मिलते हैं, पर वह सवेरे सवेरे का मिलन कुछ बहुत विशेष था। मैं चौंककर उठा था, तो एक तो जिस स्वप्न से उठा था, वह मेरे मन पर छाया था; दूसरे आँख खोलते ही सामने देखा, बगुलों की एक छोटी-सी डार आकाश में उड़ी जा रही थी, तो पहले तो मैं इसमें उलझा; स्वप्न बहुत मीठा था, उसकी मिठास बिगड़ने का डर नहीं था, बल्कि उलझने से ही डर था, यों छोड़ देने से वह और छायी जा रही थी… इसलिए बगुलों की डार से चित्त स्थिर किया। न जाने उससे क्यों एक हिलोर एक ललक मन में उठी। उसे मैंने कविता में बाँधना चाहा-कविता मुझे नहीं आती, छन्द बाँधने से तो कसीदा काढ़ता कम दुष्कर मालूम होता है; पर हाँ, आधुनिक ढंग की अनकहनी को अर्थ की बजाय ध्वनि से कहना चाहने वाली कविता से कुछ ढाढ़स बँधता है कि हाँ, यह तो हीरा-पन्ना-मोती जड़ा देव-मुकुट नहीं है, देशी पहरावा है, यह दुपल्ली शायद हम भी ओढ़ लें। तो मैंने कहना चाहा, ‘भाले की अनी-सी बनी, बगुलों की डार, फूटकियाँ छिटपुट, गोल बाँध डोलतीं, सिरहन उठती है और एकदाह में, कोई तो पधारा नहीं मेरे सूने गेह में, तुम फिर आ गये, क्वाँर देह में?’ देह में, गेह में तो बाक़ायदा तुक बन गयी; और अन्त में क्वाँर की तुक जो दूर कहीं बगुलों की डार से मिल बैठी तो जैसे स्मृति में कविता छा गयी, और कुछ पूरेपन का भाव आ गया, मुझे अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि फिर आगे नहीं सोचा; फिर स्वप्न-ही-स्वप्न था और मैं डूब गया। स्वप्न-भरी आँखें लिये-लिये ही उसके पास पहुँचा, और उससे बोला, ‘‘घूमने चलोगी? दूर लम्बी सैर को-जंगल में को चलेगी?’’
इतना तो खैर उसे जवाब का मौका देने से पहले कह गया। पर इतना ही नहीं। मन-ही-मन आगे और भी बहुत-कुछ कह गया, जैसे बगुले की डार देखकर मन-ही-मन क्वाँर से बतिया गया था, वह भी कविता में। मैंने कहा कि चलोगी, जंगल में को, जहाँ सन्नाटा है, एकान्त है, जहाँ सब अपनी-अपनी धुन में ऐसे मस्त हैं कि मस्ती की एक नयी धुन बन गयी है जिसमें सब गूँजते हैं – पर अलग-अलग, बिना एक-दूसरे पर हावी हुए जैसे शहर में होता है-शहर में जहाँ तुम कुछ ही करो, दूसरो को बड़ी दिलचस्पी है, टाँग नहीं अड़ाएँगे तो शोर मचाएँगे; और नहीं तो राह-चलते खँखारते हुए ही चले जाएँगे; जंगल में मस्त मनचले, निर्जन जंगल में चलोगी? वहाँ जहाँ कोई न होगा, वहाँ – लेकिन इतना कहकर न जाने क्यों जबान रुक जाती थी। मन ही रुक जाता था, भोर को देखा हुअ स्वप्न ही छा जाता था। स्वप्न मुझे याद था, बार-बार उभरकर याद आता था पर गूँगे के गुड़ की तरह-स्वप्न-भरी आँख से मैं अब भी देखता था कि उसमें हम-
वह चल पड़ी मेरे साथ सैर को। वह अच्छी जो है। मैं जानता हूँ। मेरे साथ-साथ चलती जा रही थी और चलते-चलते मेरे जैसे दो मन हो गये थे। एक उमंग रहा था कि वह कितनी अच्छी है और साथ है और दूसरा अभी स्वप्न की खुमारी में ही था, मीठे स्वप्न की जिसमें हम-
हम लोग जंगल में पहुँच गये। पहले, गीली-गीली, भारी-भारी, ओस से दूधिया घास-उससे भी मैंने चलते-चलते बात कर ली कि घास, ऊपर से तो चिट्टी-चिट्टी दूध-धुली, साधु-बाबा, भीतर-भीतर उमंगों से कितनी हरी हो रही है, क्या कहा है किसी ने, अरमान मचलते हैं – फिर झाड़ियाँ शुरू हो गयीं, फिर छोटे पेड़, फिर न जाने कब जंगल चुपके से घना हो गया। पहले करंज और झाऊ और ढाक, फ़िर सेमल और तूने और फिर बड़े-बड़े महा-रूख। ज़मीन भी ऊँची-नीची हो गयी, कहीं टीला, कहीं पगडंडी तो कहीं पानी की लीक, जहाँ कुछ दिन पहले नाला बहता होगा। लेकिन टीला तो उसे कहें जो खुला हो, जिसकी टांट देखी जाये, यहाँ तो सब ऐसा ढका था! फिर बीहड़ में सहसा एक थोड़ी-सी खुली जगह भी, ज़रा ऊँची मगर वैसे चिपटी, जैसे एक चौकी सी पड़ी झाड़ियों में, उस पर एक पुराना – देवी मन्दिर। मैं इतनी उमगती उदार तरंग में था कि कह गया मन्दिर, नहीं तो उस छोटी-सी, अधटूटी, काही से काली देवली को बहुत कोई माई का थान कह देता, मन्दिर; लेकिन मैंने देवी का मन्दिर ही देखा; बीहड़ वन के बीच मन्दिर; मैंने सोचा, यहाँ तान्त्रिक साधक बैठकर देवी को साधते होंगे। और उनकी साधना के औघड़ रूप भी जल्दी से मेरी दृष्टि के सामने दौड़ गये – बहुत-से, क्योंकि दृष्टि असल में तो अभी स्वप्न से आविष्ट थी, उसे साधकों की रंगी विकृतियों से क्या मतलब था, वह तो उसी स्वप्न को देख रही थी जिसमें हम-
हम… यानी वह और मैं, और मेरे साथ चली आ रही थी। बड़े भोलेपन से। उसकी आँखों में मेरी तरह दोहरी दीठ नहीं थी, वे खुली बावड़ियाँ थीं, स्वच्छ, शीतल उड़ते बादल की परछाई दिखानेवालीं। वह वैसी ही मुग्ध अपने में सम्पूर्ण मेरे साथ चली आ रही थी। मैं उसे देख लेता था, उसके साथ होने की बात सहसा मन में उभरती थी, फिर बीहड़ वन के अकेले, हरे, गीले, धुँधलेपन की, फिर मेरी आँखें उसकी आँखों की कोर से एक ढुलकी हुई लट के साथ फिसलकर उसके ओंठों तक आती थीं और फिर मेरा मन ठिठक जाता था। फिर आगे नहीं सोचता था। फिर पीछे लौट जाता था। क्योंकि पीछे स्वप्न था, स्वप्न जो पूरा था, जिस स्वप्न में हम…
तभी सामने पीछे कुछ तीखी सुरसुराहट हुई। हम ठिठक गये। सहसा वह बोली, ‘‘वह देखे सामने साँप!’’
मैंने भी देख लिया। घास के किनारे पर, मन्दिर के आस-पास की बज़री पर रेंगता हुआ, ललौंहे-भूरे रंग पर साँप था
वह गोल-गोल आँखें करके बोली, ‘‘कितना सुन्दर है साँप!’’
उसकी आँखें सचमुच बड़ी भोली थीं। डर उनमें बिलकुल नहीं था। केवल एक भोला विस्मय, एक मुग्ध भाव कि अरे, ऐसी सुन्दर चीज़ भी होती है, वह भी मिट्टी में पड़ी हुई, अनदेखी, उपेक्षित!
मैंने भी देखा। सचमुच साँप सुन्दर होता है। निर्माता की एक बड़ी सफलता है, बड़े कलाकार की प्रतिभा का एक करिश्मा-कहीं कोने नहीं, कहीं अनावश्यक रेखा नहीं, बाधा नहीं, भार नहीं, लहरीली, निरायास, लययुक्त गति, बिजली-सी त्वरा-युक्त। लेकिन बिजली की कौंध में भी कहीं नोंके होती हैं और साँप की गति निरा प्रवाह है… सुन्दर, लचीला, ललौंहा-भूरा रंग, झिलमिल चमकीली केंचुल, चित्तियाँ जो न मालूम केंचुल के ऊपर हैं कि भीतर, ऐसी काँच के भीतर झाँकती-सी जान पड़ती हैं…
मैंने तो देख लिया। फिर मैं उसे देखने लगा, और वह साँप को देखती रही। हम दोनों जैसे मन्त्रमुग्ध थे, लेकिन एक ही मन्त्र से नहीं। वह साँप को देखती थी, मैं उसे देखता था। वह साँप के लयमय प्रवाह पर विस्मय कर रही थी, मैं उसके चेहरे की मानो क्षण-भर के लिए थम गयी चंचल बिजलियों को देख रहा था और सोच रहा था, कोने एक-दूसरे को काटते हैं, पर लहरीली गतिमान रेखाएँ काटतीं नहीं, झट से कौंधकर मिल जाती हैं, बिजली की कौंध तो है ही लय होने के लिए; लहर को देखो और खो जाओ, डूब जाओ, लय हो जाओ। उसकी आँखें साँप पर टिककर मुग्ध थीं। मेरी आँखों में मेरे भोर में देखे हुए स्वप्न की खुमारी थी। स्वप्न में इसी तरह देखा था कि…
साँप आगे बढ़ गया। मन्दिर की दीवार के साथ सट गया, ऐसा सटकर चिपक गया कि बस-जैसे मन्दिर की रेखा से अलग उसकी रेखा नहीं है, जैसे मन्दिर की नींव से ही वह सटा हुआ उठा है और वैसा ही रहेगा।
और चिपके-चिपके भी वह स्थिर नहीं था, वह आगे सरक रहा था। आगे-आगे, और गहरा चिपकता हुआ। जैसे उसकी देह की रगड़ की आरी से कटकर मन्दिर की दीवार के नीचे उसके लिए जगह बनती जाती हो और उसमें वह धँसता-पैठता जाता हो।
बढ़ता हुआ वह हमारे सामने की दीवार के कोने तक बढ़कर दूसरी दीवार के साथ मुड़ चला। थोड़ा और बढ़ा, फिर रुक गया। आधा इस दीवार के साथ जो हमारे सामने थी; आधा साथ की, जो हमारी ओट थी। उसका सिर ओट में हो गया, कमर दोनों दीवारों के जोड़ पर टिक गयी।
मैंने सहसा कहा, ‘‘इस वक्त यह कैसा वेध्य है। अगर मैं मारना चाहूँ, तो निरीह मर जाये-’’
‘‘हाँ, लेकिन क्यों मारना चाहो? इतना सुन्दर-’’
मैंने अपनी ही झोंक में कहा, ‘‘अभी ढेला मारूँ, तो बस, काटने को मुड़ भी न सके-’’
‘‘क्या ज़हरीला है?’’
‘‘हो भी तो क्या? इस समय असहाय है, मौके की बात है, कुछ कर भी न सके, सारा रूप लिए ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाए बिटुर-बिटुर तकता!’’
उसकी पहले ही मुग्ध गोल आँखें करुणा से और बड़ी-बड़ी हो आयीं। बोली, ‘‘बेचारा कितना असहाय!’’ कितनी करुणा थी उस स्वर में, कितना निरीह था वह स्वर भी शायद साँप से अधिक निरीह! स्वप्न में मैंने देखा था वह और मैं – हम – लेकिन स्वप्न की उलझन – जैसे सुलझ गयी, मेरी दोहरी दीठ इकहरी हो गयी और मैंने देखा, मैं अलग यहाँ, वह अलग वहाँ, और हम दोनों खड़े उस सुन्दर चित्तीदार ललौहें-भूरे, लचीली लहर से बल खाते साँप को देखते रहे। मैं भी, वह भी। चाहे मैं साँप को जितना देख रहा था, उससे अधिक उसी को देख रहा था। साँप तो मन्दिर की भीत से सटा खड़ा था, और वह मुझसे सटी खड़ी थी।
फिर मैंने कहा, ‘‘चलो, आगे चलें।’’
हम लोग चल पड़े। पर असल में आगे हम नहीं चले, हम लौट आये। वह बीहड़ में मन्दिर वहीं खड़ा रह गया। तान्त्रिक वहाँ कभी अपनी औघड़-पूजा किया करते होंगे, किया करें। उन्होंने वैसा सुन्दर साँप कभी थोड़े ही देखा होगा – कम-से-कम उतना असहाय और वेध्य? यों तो मैंने भी कभी नहीं देखा, स्वप्न में भी नहीं, यद्यपि सपने मैंने एक-से-एक सुन्दर देखे हैं, जिन्हें मैं कह भी नहीं सकता। और किसी को तो क्या, उसको भी नहीं, जो मैं जानता हूँ कि इतनी अच्छी है, चाहे मैं अच्छा होऊँ या बुरा।



![kuber chalisa[1]](https://mobihangama.com/wp-content/uploads/2022/09/Kuber-Chalisa1-300x225.jpg)